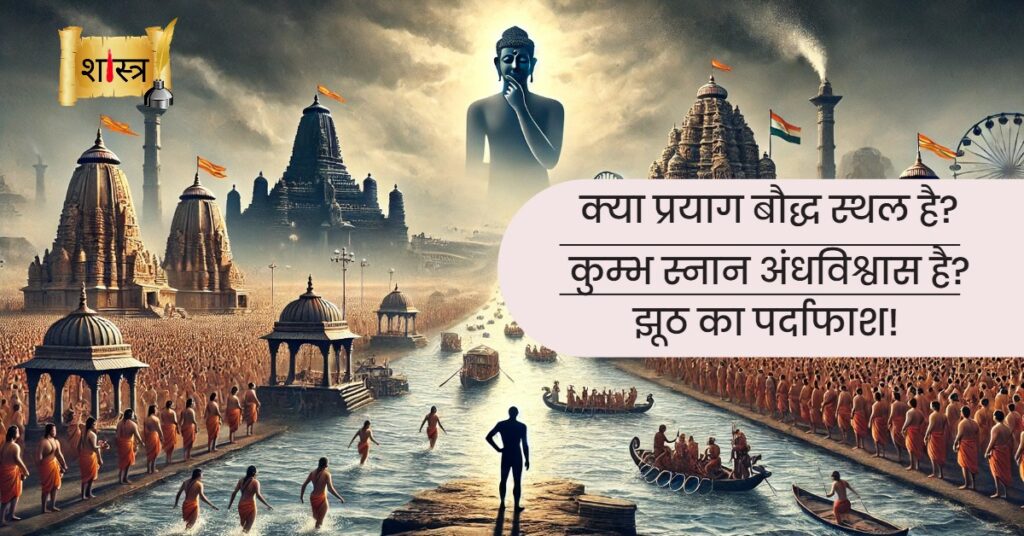भूमिका: कैसे पाखंडी बुद्धिजीवी प्रयाग और कुंभ स्नान को बदनाम कर रहे हैं?
आजकल कुछ तथाकथित ‘बुद्धिजीवी’ प्रयागराज (प्रयाग) को बौद्ध स्थल बताने की कोशिश कर रहे हैं और महाकुंभ स्नान को अंधविश्वास करार दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जो सनातन संस्कृति और परंपराओं पर झूठ फैलाते हैं, बिना किसी ऐतिहासिक प्रमाण के। उनका दावा है कि प्रयाग का असली इतिहास बौद्ध धर्म से जुड़ा है और महाकुंभ केवल एक काल्पनिक परंपरा है, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इस लेख में हम इन झूठे दावों का न केवल खंडन करेंगे, बल्कि प्रामाणिक ग्रंथों और वैज्ञानिक अनुसंधानों के माध्यम से सनातन संस्कृति की सच्चाई को उजागर करेंगे।
इस विषय में हमारा यह वीडियो द्रष्टव्य है –
अफवाह की उत्पत्ति: प्रयाग को बौद्ध स्थल क्यों बताया गया ?
यह झूठी अफवाहें फैलाने के पीछे एक गहरी साजिश है, जिसका मुख्य स्रोत पश्चिमी औपनिवेशिक विद्वानों की गलत व्याख्याएं हैं।
1. अलेक्जेंडर कनिंघम की गलत व्याख्या और पक्षपात
अलेक्जेंडर कनिंघम, जो ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता थे, ने अपनी पुस्तक “Ancient Geography of India” में प्रयाग को एक बौद्ध स्थल मानने की कोशिश की। उनके शब्दों में देखिए पृष्ठ 262 पर (अंग्रेजी पुस्तक में पृष्ठ 436 पर) –


कन्निंघम की पुस्तक आप यहाँ से डाऊनलोड कर सकते हैं –


लेकिन उनकी यह व्याख्या उनके कोलोनियल मानसिकता से ग्रस्त होने और भारतीय संस्कृति के इतिहास से अनभिज्ञता का परिचायक है। उनकी शोध में बौद्ध स्थलों को अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति थी, क्योंकि ब्रिटिश प्रशासन की रुचि हिन्दू धर्म का प्रभाव कम करने में थी |
2. ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत और बौद्ध पूर्वाग्रह
चीन के यात्री ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की और अपने यात्रा वृतांत में प्रयाग का उल्लेख किया। उनका कहना था की प्रयाग कभी बौद्ध धर्म का केंद्र था।

ह्वेनसांग की भारत यात्रा की पुस्तक आप यहाँ से डाऊनलोड कर सकते हैं –

ह्वेनसांग स्वयं बौद्ध भिक्षु थे भारत बौद्ध धर्म के विषय में जानने आये थे | किसी भी विषय पर अन्य मतों पर पर्याप्त शोध करना अथवा उनका उल्लेख करना भी उनके लिए आवश्यक नहीं था |अतएव उन्होंने अधिकतर बौद्ध स्थलों का ही विवरण दिया, जिससे उनका विवरण पक्षपाती हो सकता है।
ऋग्वेद से प्रमाण: सनातन संस्कृति में प्रयाग का महत्व
ऋग्वेद में नदी सूक्त (ऋग्वेद 10.75.5) में स्पष्ट रूप से गंगा, यमुना और सरस्वती का उल्लेख मिलता है:

श्री राम शर्मा आचार्य का भी अनुवाद देखें –

महाभारत से प्रमाण: संगम स्नान का धार्मिक महत्त्व
महाभारत के वन पर्व में प्रयाग का वर्णन आया है | वहाँ संगम स्नान की भी चर्चा आयी है | दरअसल प्रयाग के नाम से ही प्रकृष्ट याग (यज्ञ) का बोध होता है जिसका महत्त्व सनातन परंपरा में है, न की बौद्ध परंपरा में |
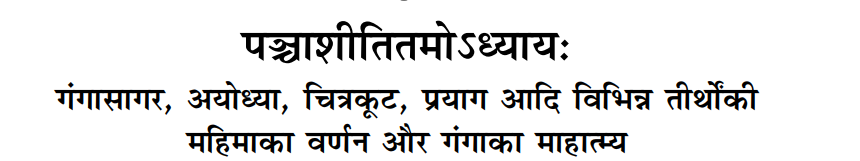


गीताप्रेस से छः खण्डों में महाभारत प्रकाशित होती है जिसके दूसरे खंड में वन पर्व आया है | इसे आप यहाँ से डाऊनलोड कर सकते हैं –
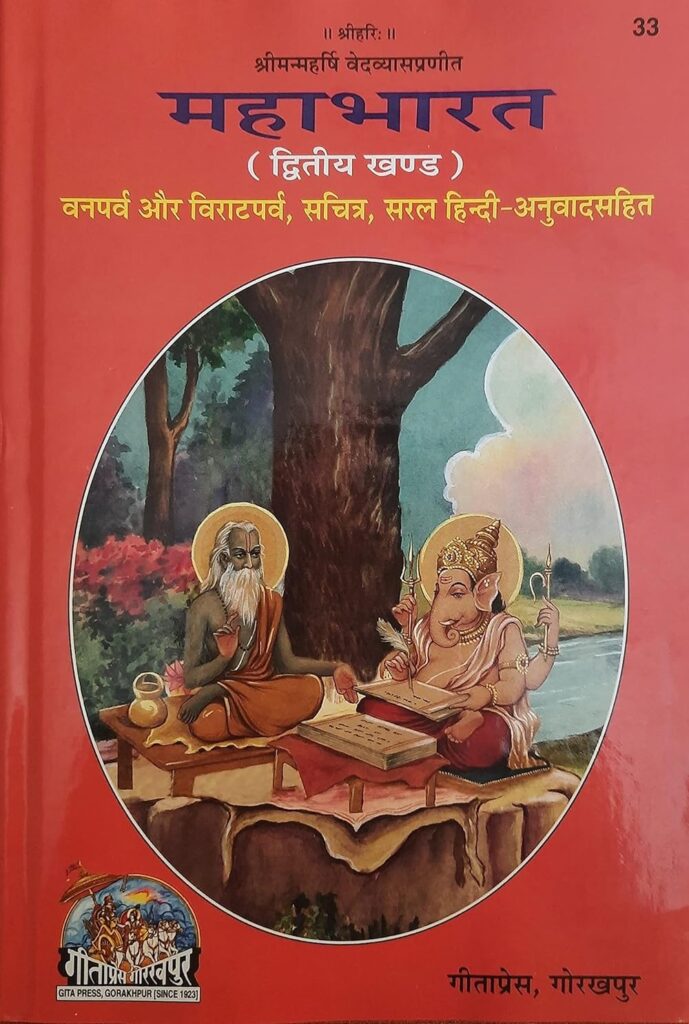
E-Book Version:
क्या बौद्ध धर्म में नदी स्नान का धार्मिक महत्त्व है?
भगवान् बुद्ध ने नदी स्नान से किसी आध्यात्मिक लाभ को इंकार किया है | यह बात त्रिपिटक से प्रमाणित होती है |
त्रिपिटक तीन हैं – सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक |
सुत्त पिटक के संयुत्त निकाय में सुन्दरिक सुत्त आया है | इसमें सुन्दरिका नदी के तट पर भगवान् बुद्ध का सुन्दरिक नामक ब्राह्मण से वार्ता होती है | इसमें भगवान् बुद्ध स्वयं आध्यात्मिक स्नान के बारे में बताते हैं –



संयुत्त निपात पर द्वारिकादास शास्त्री की तीन खण्डों में अनुवाद आती है | उसके पहले खंड के पृष्ठ 271 में यह सुन्दरिक सुत्त आया है जिसे आप यहाँ से डाऊनलोड कर सकते हैं –

इसलिए कुम्भ स्नान बौद्धों का पर्व हो ही नहीं सकता क्योंकि भगवान् बुद्ध नदी स्नान का कोई विशेष महत्त्व नहीं मानते थे |
दरअसल ऐसा मानने में उनकी भी कोई गलती नहीं थी | पिछले दस पंद्रह वर्षों में डॉक्टर एंड्रू न्यूबर्ग जैसे न्यूरोसाइंटिस्ट ने विज्ञान की न्यूरोथिओलॉजी (Neurotheology) नामक एक शाखा को जन्म दिया है | यह शाखा बुद्ध के समय थी ही नहीं अतएव वह इससे अनभिज्ञ थे |

Dr. Andrew Newberg, MD Uni of Pennsylvania, Neuroscientist
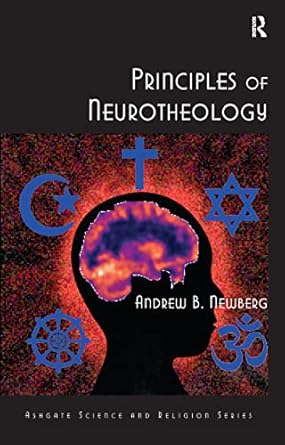
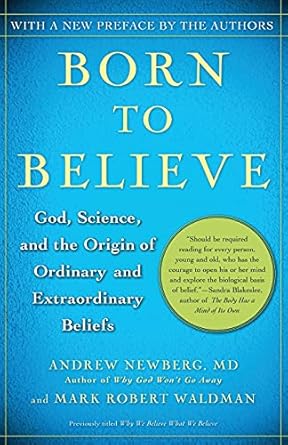
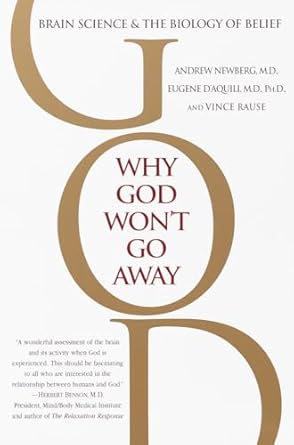
उनका कहना है कि दिमाग पर fMRI स्कैन और न्यूरोसाइंस के साक्ष्य यह सिद्ध करते हैं कि धार्मिक कर्म काण्ड का दिमाग पर सकारात्मक असर पड़ता है चाहे उनका कोई तार्किक मूल्य हो या न हो | अतएव जो छद्म बुद्धिजीवी धर्म ग्रंथों की बातों को असंभव माइथोलॉजी और गपोड़ा कह के खारिज कर देते हैं उन्हें न्यूरोथिओलॉजी (Neurotheology) का कुछ भी नहीं पता ! शास्त्रों की उन बातों का कोई अर्थ हो न हो, वे मानव मस्तिष्क के लाभदायक हैं ऐसा एंड्रू न्यूबर्ग प्रभृति विद्वानों का कहना है |
भगवान् बुद्ध ने तीर्थ स्नान को शायद इसलिए व्यर्थ कह दिया होगा की इससे निब्बान नहीं मिल सकता होगा !
वैज्ञानिक शोध: कुंभ मेले में भाग लेने के लाभ
इस विषय में यह शोध द्रष्टव्य है जो मनोविज्ञान क्षेत्र के विशेषज्ञों ने किया है –

यह शोध Economic and Social Research Council (ESRC) द्वारा वित्तपोषित किया गया था और इसे श्रुति तिवारी (Centre of Behavioural and Cognitive Sciences, University of Allahabad), समीह खान (School of Psychology, University of Dundee), निक हॉपकिंस (University of Dundee), नारायणन श्रीनिवासन (University of Allahabad), और स्टीफन रीचर (School of Psychology, University of St Andrews) द्वारा किया गया। इस अध्ययन का उद्देश्य यह समझना था कि कुम्भ मेले जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों में भाग लेने से प्रतिभागियों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य, सामाजिक व्यवहार, और सामूहिक चेतना पर क्या प्रभाव पड़ता है।
शोध की नैतिकता और निष्पक्षता
यह अध्ययन University of Dundee और University of Allahabad की Ethics Committees द्वारा अनुमोदित था। प्रतिभागियों को पूरी जानकारी देने के बाद उनकी मौखिक सहमति ली गई, क्योंकि इनमें से कई प्रतिभागी लिखित सहमति देने में सक्षम नहीं थे। ESRC ने केवल वित्तपोषण प्रदान किया था और शोध में हस्तक्षेप नहीं किया, जिससे इसके निष्कर्ष पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र हैं।
शोध की प्रक्रिया और निष्कर्ष
शोधकर्ताओं ने 2011 के माघ मेले में भाग लेने वाले 416 कल्पवासी और 127 नियंत्रण समूह (जो मेले में नहीं गए) का अध्ययन किया।
- डेटा संग्रह (Data Collection): डेटा दो चरणों में एकत्र किया गया:
- T1: माघ मेले से एक महीने पहले
- T2: माघ मेले के एक महीने बाद
- मनोवैज्ञानिक प्रश्नावली: प्रतिभागियों से उनकी शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति, ऊर्जा स्तर और स्वास्थ्य से संबंधित लक्षणों के बारे में 5-पॉइंट स्केल के माध्यम से डेटा लिया गया।
- आमने-सामने साक्षात्कार: हिंदी बोलने वाले प्रशिक्षित फील्ड अन्वेषकों की टीम ने प्रतिभागियों से बातचीत की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सर्वे स्पष्ट और आसानी से समझने योग्य हो।
शोध सार:
शोध से पता चला कि कल्पवासी, जिन्होंने पूरे महीने माघ मेले में भाग लिया, उन्होंने अपना मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की संतोषजनक भावना को नियंत्रण समूह की तुलना में अधिक बढ़ाया।
- T1 और T2 के बीच कल्पवासियों की शारीरिक और मानसिक स्थितियों में उल्लेखनीय सुधार देखा गया।
- स्वास्थ्य संबंधी लक्षणों में कमी आई, जैसे चिंता, चिड़चिड़ापन, और शारीरिक दर्द।
- सामूहिक भागीदारी ने प्रतिभागियों को सामाजिक समर्थन और सामूहिक पहचान की भावना दी, जिससे उनका सामाजिक लचीलापन (resilience) बढ़ा।
- धार्मिक आयोजन केवल आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य में सुधार और सामूहिक चेतना को मजबूत करने में भी सहायक हैं।
- ऐसे आयोजन प्रतिभागियों को सामाजिक पहचान और सहयोग की भावना देते हैं, जिससे वे सकारात्मक जीवन दृष्टिकोण विकसित करते हैं।


यह शोध कुम्भ स्नान को अंधविश्वास कहने वालों के लिए एक करारा जवाब है। यह साबित करता है कि धार्मिक अनुष्ठानों का वैज्ञानिक आधार भी है, जो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यंत लाभकारी हैं।
निष्कर्ष: प्रयाग सनातन का केंद्र और कुंभ स्नान का वैज्ञानिक महत्व
इस लेख में हमने स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया:
✅ ऋग्वेद, महाभारत और अन्य हिंदू ग्रंथों में प्रयाग का उल्लेख है।
✅ बौद्ध ग्रंथों से ही सिद्ध होता है कि बुद्ध नदी स्नान के विरुद्ध थे।
✅ न्यूरोथियोलॉजी और आधुनिक वैज्ञानिक शोध साबित करते हैं कि महाकुंभ केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक रूप से भी लाभकारी है।
✅ कनिंघम और ह्वेनसांग के विवरण पूर्वाग्रह से भरे हुए थे और इन्हें ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता।
जो लोग प्रयाग और महाकुंभ को बदनाम कर रहे हैं, उनके झूठों की पोल अब खुल चुकी है!
🚩 सनातन का सम्मान करें, अपने गौरवशाली इतिहास को जानें! 🚩